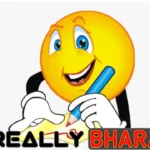बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है ? इसके पीछे की वजहें
पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान लंबे समय से अशांति और विद्रोह का केंद्र बना हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) जैसे संगठनों के नेतृत्व में बलूच लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। इस मांग के पीछे ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों का एक जटिल मिश्रण है, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बनाता है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: जबरन कब्जे की कहानी
बलूचिस्तान का इतिहास 1947 के भारत विभाजन से शुरू होता है। उस समय, बलूचिस्तान (जिसमें कलात, खारान, लास बेला और मकरान की रियासतें शामिल थीं) ने स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई थी। 11 अगस्त 1947 को कलात के खान और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें कलात को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी गई। हालांकि, यह स्वतंत्रता केवल 227 दिन तक ही कायम रही। 1948 में पाकिस्तानी सेना ने सैन्य अभियान चलाकर बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा कर लिया। इस घटना ने बलूचों में अलगाव की भावना को जन्म दिया, जो आज तक कायम है।
बलूचिस्तान का आर्थिक शोषण और भेदभाव
बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे संसाधन-संपन्न प्रांत है, जहां तेल, गैस, सोना, तांबा और अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह प्रांत देश की 40% से अधिक गैस का उत्पादन करता है। फिर भी, यह पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, जहां 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। स्थानीय बलूचों का आरोप है कि उनके संसाधनों का दोहन पंजाब और सिंध जैसे अन्य प्रांतों के विकास के लिए किया जाता है, जबकि बलूचिस्तान को इसका कोई लाभ नहीं मिलता।
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) और ग्वादर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स ने इस असंतोष को और बढ़ाया है। बलूचों का मानना है कि इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को न तो रोजगार मिला और न ही आर्थिक विकास हुआ। इसके विपरीत, ग्वादर पोर्ट को चीन के हवाले करने से बलूचों में अपनी जमीन और संसाधनों के हड़पने का डर बढ़ गया है।
बलूचिस्तान का सांस्कृतिक और जातीय पहचान का संकट
बलूच लोग अपनी भाषा (बलूची), संस्कृति और इतिहास को पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से अलग मानते हैं। उनकी सभ्यता को 5,000 साल पुराना माना जाता है और वे इसे पाकिस्तान की मुख्यधारा की उर्दू और पंजाबी संस्कृति से जोड़ना नहीं चाहते। बलूचों को डर है कि पाकिस्तानी सरकार उनकी सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस कारण वे बाहरी लोगों, खासकर पंजाबियों के बलूचिस्तान में आने का विरोध करते हैं।
बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन और सैन्य दमन
बलूच कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार ने उनके खिलाफ दमनकारी नीतियां अपनाई हैं। जबरन गायब किए जाना, अपहरण, टॉर्चर और हत्याओं के मामले आम हैं। 2006 में बलूच नेता नवाब अकबर बुगती की हत्या ने इस विद्रोह को और भड़काया। इसके अलावा, बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों को पाकिस्तान सरकार आतंकवादी मानती है और उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों को तेज करती है, जिससे हिंसा का चक्र और बढ़ता है।
हाल की घटनाएं और बढ़ता तनाव
हाल के वर्षों में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना और CPEC से जुड़े ठिकानों पर हमलों को तेज किया है। मई 2025 में BLA ने क्वेटा में एक सैन्य वाहन पर हमला कर 12 सैनिकों को मारने का दावा किया। इसके अलावा, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण जैसी घटनाओं ने बलूचों की मांग को वैश्विक ध्यान दिलाया है। ये हमले न केवल बलूचों की नाराजगी को दर्शाते हैं, बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गए हैं।
बलूचिस्तान को लेकर अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण
बलूचिस्तान की आजादी की मांग ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा है। 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाया था, जिससे इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर जगह मिली। कुछ बलूच नेता भारत से सैन्य या नैतिक समर्थन की उम्मीद करते हैं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय मान्यता के बिना बलूचिस्तान का स्वतंत्र देश बनना मुश्किल है।
बलूचिस्तान की भविष्य की संभावनाएं
बलूचिस्तान की स्थिति दिन-ब-दिन जटिल होती जा रही है। पाकिस्तान सरकार बातचीत के बजाय सैन्य कार्रवाई पर जोर दे रही है, जिससे बलूचों का असंतोष और बढ़ रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि पाकिस्तान ने बलूचों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, तो यह स्थिति 1971 के बांग्लादेश संकट जैसी हो सकती है।